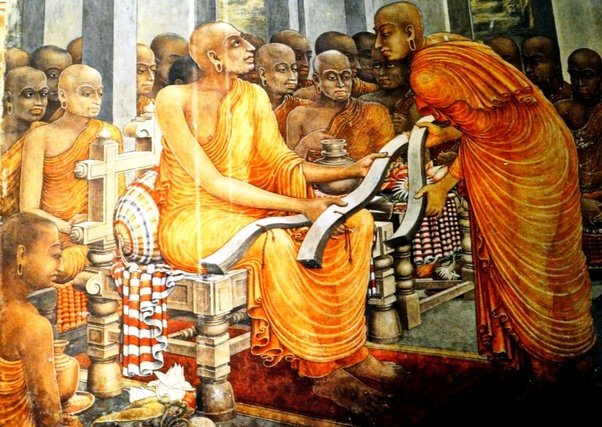चित्त
चित्त विशेष रूप से मन या चेतना (Consciousness) को कहते हैं। यह वह तत्व है जो अनुभव, संज्ञान (cognition) और भावनाओं को उत्पन्न करता है। यह निरंतर परिवर्तनशील और क्षणभंगुर होता है। चित्त के विषय में कहा जाता है कि ‘चित्तं नाम चेतनस्स हेतु’ अर्थात् चित्त वह है जो चेतना को उत्पन्न करता है। चित्त किसी भी अनुभव को ग्रहण करने, उसे समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। चित्त का गहन अध्ययन करने से व्यक्ति ध्यान की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है, जिससे वह आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है।
चित्त के प्रमुख गुण
- अनित्य (Anicca) – चित्त हर क्षण बदलता रहता है।
- दुःख (Dukkha) – यह परिवर्तनशीलता के कारण अस्थिर और अप्रत्याशित अनुभवों को जन्म देता है।
- अनात्म (Anatta) – चित्त का कोई स्थायी ‘स्वरूप’ नहीं होता, यह विभिन्न मानसिक कारकों (चेतसिक) के साथ मिलकर कार्य करता है।
चित्त के प्रकार
चित्त को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है —
- कुसल चित्त (Kusala Citta) – इसे पुण्यकारी चित्त कहते हैं। यह शील, ध्यान और प्रज्ञा को बढ़ाने वाला है। जैसे— दान देने का चित्त आदि।
- अकुसल चित्त (Akusala Citta) – इसे अपुण्यकारी चित्त कहते हैं। यह लोभ, दोस और मोह के कारण उत्पन्न होता है। जैसे— क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार से उत्पन्न चित्त।
- विपाक चित्त (Vipāka Citta) – इसे फलदायक चित्त कहते हैं। यह पूर्वकृत कर्मों का परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला चित्त होता है। जैसे— पिछले कर्म के पुण्य या पाप के अनुसार मिलने वाले अनुभव।
- किरिया चित्त (Kiriya Citta) – इसे निष्क्रिय चित्त कहते हैं। यह किसी कर्म का फल उत्पन्न नहीं करता, केवल मानसिक कार्य के रूप में रहता है। जैसे — अर्हतों (बुद्धत्व प्राप्त व्यक्तियों) का चित्त, जो कर्मबंधन से मुक्त होता है।
चित्त और मानसिक कारक
चित्त अकेले कार्य नहीं करता, बल्कि यह 52 मानसिक कारकों के साथ मिलकर कार्य करता है। ये मानसिक कारक चित्त को दिशा, भावना और प्रभाव प्रदान करते हैं। जैसे— लोभ सहगत चित्त, दोस सहगत चित्त और मोह सहगत चित्त आदि।
चित्त का प्रवाह (चित्त-संतति)
विपश्यना के अभ्यास में चित्त को एक निरंतर प्रवाह (चित्त-संतति) के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक चित्त क्षणिक होता है और एक चित्त के समाप्त होते ही दूसरा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में चित्त की तीन अवस्थाएँ होती हैं—
- उप्पाद (Uppāda) – चित्त की उत्पत्ति
- ठिति (Thiti) – चित्त की स्थिति (अति अल्पकालिक)
- भंग (Bhanga) – चित्त का विलय (अवसान)
यह निरंतरता अनात्मवाद का समर्थन करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं होती, बल्कि चित्त मात्र एक मानसिक प्रवाह है।
अभिधम्मत्थसंगहो के अनुसार चित्त का वर्गीकरण
- कामावचर चित्त (कामधातु में कार्य करने वाला चित्त)
- रूपावचर चित्त (रूपध्यान से संबंधित चित्त)
- अरूपावचर चित्त (अरूपध्यान से संबंधित चित्त)
- लोकुत्तर चित्त (निर्वाण से संबंधित चित्त)
संक्षिप्त विवरण
- कामावचर चित्त (काम-लोक में कार्य करने वाला चित्त)
- अकुसल चित्त (12 प्रकार) – लोभ, द्वेष, मोहजन्य चित्त।
- अहेतुक चित्त (18 प्रकार) – इंद्रिय-द्वारों से उत्पन्न होने वाले चित्त।
- सोभन चित्त (कामावचर कुसल, विपाक, किरिया – 24 प्रकार) – पुण्यकारी चित्त।
- रूपावचर चित्त (ध्यान से संबंधित चित्त)
- ध्यान के पाँच स्तरों के आधार पर 15 चित्त।
- अरूपावचर चित्त (सूक्ष्म ध्यान से संबंधित चित्त)
- चार ध्यान अवस्थाओं के अनुसार 12 चित्त।
- लोकुत्तर चित्त (निर्वाण से संबंधित चित्त)
- आर्य मार्ग के आठ चरणों के अनुसार 8 चित्त।
सोमनस्ससहगतं
- सोमनस्स + सहगतं
- सोमनस्स (Somanassa)
- सोम (शांत, प्रसन्न) + मनस्स (मन)
- अर्थात प्रसन्नचित्तता, सुखपूर्ण मनोदशा
- सहगतं (Sahagataṁ)
- सह (साथ) + गत (गमन) + अं (तद्धित प्रत्यय)
- अर्थात साथ रहने वाला, संलग्न, सहचरित
अन्वय
- सोमनस्ससहगतं = सोमनस्सेन सह गतं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो सुखानुभूति के साथ प्रवाहित होता है।
अर्थ
‘सोमनस्ससहगतं चित्त’ वह चित्त है जो आनंद, प्रसन्नता और सुखमय भावना के साथ उत्पन्न होता है। यह सुख-वेदना (सांसारिक या आध्यात्मिक प्रसन्नता) से युक्त होता है और सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं (जैसे कुसल चित्त) में देखा जाता है।
दिट्ठिगतसम्पयुत्तं
- दिट्ठिगत + सम्पयुत्तं
- दिट्ठिगत (Diṭṭhigata)
- दिट्ठि (दृष्टि, मत, विचार) + गत (स्थित, संबद्ध)
- अर्थात किसी विशेष दृष्टिकोण, मत या विचार से संबंधित।
- विशेष रूप से यह शब्द मिथ्यादृष्टि (गलत दृष्टिकोण) के लिए प्रयुक्त होता है, जो बौद्ध दर्शन में दृष्टिग्राह्यता (view attachment) या दृढ़ मताग्रह (wrong belief attachment) को दर्शाता है।
- सम्पयुत्तं (Sampayuttaṁ)
- सम् (साथ) + पयुत्त (संलग्न, संबद्ध) + अं (तद्धित प्रत्यय)
- अर्थात किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ, संबद्ध।
अन्वय
- दिट्ठिगतसम्पयुत्तं = दिट्ठिगतस्स सह सम्पयुत्तं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो किसी विशेष दृष्टिकोण (विशेषकर मिथ्यादृष्टि) के साथ संबद्ध होता है।
अर्थ
‘दिट्ठिगतसम्पयुत्तं चित्त’ वह चित्त है जो मिथ्यादृष्टि (गलत दृष्टिकोण) के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह लोभमूलक चित्तों का एक प्रकार है, जहाँ व्यक्ति किसी गलत विश्वास, संकीर्ण दृष्टिकोण या भ्रांत धारणाओं से चिपका रहता है। यह शब्द मुख्य रूप से अकुसल चित्तों (अशुभ चित्तों) में आता है, जहाँ किसी व्यक्ति की सोच अहंकार, मोह या लोभ के कारण विकृत हो जाती है और वह सत्य को गलत तरीके से समझने लगता है।
संक्षिप्त सार
दिट्ठिगतसम्पयुत्तं चित्त = विकृत दृष्टिकोण (मिथ्यादृष्टि) से संबद्ध चित्त।
असङ्खारिकमेकं
- असङ्खारिक + एकं
- असङ्खारिक (Asaṅkhārika)
- अ (नकारार्थक उपसर्ग) + सङ्खारिक (प्रयत्नशील, प्रेरित, योजना करने वाला)
- सङ्खारिक (Saṅkhārika) शब्द संखार (saṅkhāra) से बना है, जिसका अर्थ होता है— संयोजन, तैयारी, प्रयास, प्रेरणा।
- अतः असङ्खारिक का अर्थ हुआ— जो बिना किसी बाहरी प्रेरणा, योजना या प्रयास के उत्पन्न हुआ हो, अर्थात स्वतः उत्पन्न होने वाला चित्त।
- एकं (Ekaṁ)
- एक (एक, अकेला) + अं (तद्धित प्रत्यय)
- अर्थात एक प्रकार का, एकमात्र।
अन्वय
- असङ्खारिकमेकं = असङ्खारिकं चित्तं एकं
- अर्थात ऐसा एक चित्त जो बिना किसी बाहरी प्रेरणा के स्वयं उत्पन्न होता है।
अर्थ
‘असङ्खारिक चित्त’ वह चित्त है जो स्वतः उत्पन्न होता है, बिना किसी बाहरी प्रेरणा या प्रयास के। यह ससङ्खारिक चित्त (जो किसी बाहरी प्रेरणा, सोच-विचार या परामर्श से उत्पन्न होता है) के विपरीत है।
संक्षिप्त सार
असङ्खारिकमेकं चित्त = स्वतः उत्पन्न होने वाला चित्त, बिना किसी प्रेरणा या योजना के उत्पन्न हुआ एक चित्त। यह अभिधम्म में अकुसल (अशुभ) और कुसल (शुभ) दोनों प्रकार के चित्तों में आता है।
ससङ्खारिकमेकं
- ससङ्खारिक + एकं
- ससङ्खारिक (Saṅkhārika)
- स (साथ) + सङ्खारिक (प्रयत्नशील, प्रेरित, योजना करने वाला)
- सङ्खार (Saṅkhāra) शब्द सं+खृ (संघटित करना, बनाना, तैयार करना) धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है— प्रयास, योजना, प्रेरणा, संकल्प।
- अतः ससङ्खारिक का अर्थ हुआ— जो किसी बाहरी प्रेरणा, योजना या प्रयास से उत्पन्न हुआ हो, अर्थात प्रयासपूर्वक उत्पन्न होने वाला चित्त।
- एकं (Ekaṁ)
- एक (एक, अकेला) + अं (तद्धित प्रत्यय)
- अर्थात एक प्रकार का, एकमात्र।
अन्वय
- ससङ्खारिकमेकं = ससङ्खारिकं चित्तं एकं
- अर्थात ऐसा एक चित्त जो बाहरी प्रेरणा, योजना या प्रयास से उत्पन्न होता है।
अर्थ
‘ससङ्खारिक चित्त’ वह चित्त है जो बाहरी प्रेरणा, योजना, अथवा संकल्प से उत्पन्न होता है। यह असङ्खारिक चित्त (जो बिना किसी बाहरी प्रेरणा के स्वतः उत्पन्न होता है) के विपरीत है। ससङ्खारिक चित्त किसी अन्य व्यक्ति के उपदेश, विचार, प्रेरणा, अथवा किसी आंतरिक योजना के कारण उत्पन्न हो सकता है।
संक्षिप्त सार:
ससङ्खारिकमेकं चित्त = बाहरी प्रेरणा या योजना से उत्पन्न हुआ एक चित्त।
यह अभिधम्म में अकुसल (अशुभ) और कुसल (शुभ) दोनों प्रकार के चित्तों में आता है।
दिट्ठिगतविप्पयुत्तं
- दिट्ठिगत + विप्पयुत्तं
- दिट्ठिगत (Diṭṭhigata)
- दिट्ठि (दृष्टि, मत, विचार) + गत (स्थित, संबद्ध)
- अर्थात किसी विशेष दृष्टिकोण, मत या विचार से संबंधित।
- विशेष रूप से यह शब्द मिथ्यादृष्टि (गलत दृष्टिकोण) के लिए प्रयुक्त होता है, जो बौद्ध दर्शन में दृष्टिग्राह्यता (view attachment) या दृढ़ मताग्रह (wrong belief attachment) को दर्शाता है।
- विप्पयुत्तं (Vippayuttaṁ)
- वि (विरुद्ध, अलग) + पयुत्त (संलग्न, संबद्ध) + अं (तद्धित प्रत्यय)
- अर्थात अलग, असंबद्ध, मुक्त।
अन्वय
- दिट्ठिगतविप्पयुत्तं = दिट्ठिगतस्स विप्पयुत्तं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो किसी विशेष दृष्टिकोण (विशेषकर मिथ्यादृष्टि) से मुक्त हो।
अर्थ
‘दिट्ठिगतविप्पयुत्तं चित्त’ वह चित्त है जो मिथ्या दृष्टि (गलत दृष्टिकोण) से मुक्त होता है। यह दिट्ठिगतसम्पयुत्तं चित्त (जो मिथ्या दृष्टि से संबद्ध होता है) के विपरीत है। इस प्रकार का चित्त निष्पक्ष होता है और किसी भी गलत विश्वास, संकीर्ण दृष्टिकोण या भ्रांत धारणाओं से प्रभावित नहीं होता।
संक्षिप्त सार:
दिट्ठिगतविप्पयुत्तं चित्त = मिथ्यादृष्टि से मुक्त चित्त।
यह चित्त निष्पक्ष होता है और किसी गलत मताग्रह से प्रभावित नहीं होता।
‘उपेक्खासहगतं’
- उपेक्खा + सहगतं
- उपेक्खा (Upekkhā)
- उप (समीप, समान) + इक्ख (√ikkh) (देखना, निरीक्षण करना) + आ (प्रत्यय)
- अर्थात समभाव, तटस्थता, निष्पक्ष दृष्टिकोण।
- यह न तो सुख (सोमनस्स) और न ही दुख (दुक्ख) से युक्त अनुभूति होती है।
- सहगतं (Sahagataṁ)
- सह (साथ) + गत (गमनशील, संयुक्त) + अं (तद्धित प्रत्यय)
- अर्थात जिसके साथ संयुक्त हो, जिसमें सम्मिलित हो।
अन्वय
- उपेक्खासहगतं = उपेक्खाय सहगतं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो समभाव या तटस्थता के साथ संयुक्त हो।
अर्थ
‘उपेक्खासहगतं चित्त’ वह चित्त है जो तटस्थता, समता और मानसिक संतुलन के साथ जुड़ा होता है। यह चित्त न सुख (सोमनस्स) न दुख (दुक्ख) की भावना से प्रभावित होता है। यह विशेष रूप से ध्यान में देखा जाता है, जहाँ व्यक्ति न आसक्ति (राग) न द्वेष (द्वेष) की ओर झुकता है।
संक्षिप्त सार:
उपेक्खासहगतं चित्त =
तटस्थता और समभाव से युक्त चित्त।
यह न सुखद (pleasurable) न दुखद (painful) होता है, बल्कि समता की स्थिति में रहता है।
लोभसहगतचित्तानि
- लोभ + सहगत + चित्तानि
- लोभ (Lobha)
- √लुभ् (लुभ्यते) धातु से बना हुआ शब्द।
- इसका अर्थ होता है अधिक पाने की इच्छा, तृष्णा, लालच या आसक्ति।
- बौद्ध दर्शन में यह तीन अकुशल मूलों (अकुसल मूल) में से एक है— लोभ, द्वेष और मोह।
- सहगत (Sahagata)
- सह (साथ) + गत (गमनशील, संयुक्त)
- अर्थात जो किसी चीज़ के साथ जुड़ा हो, जिसमें सम्मिलित हो।
- चित्तानि (Cittāni)
- चित्त (मन, चेतना, मानसिक अवस्था) + आनि (बहुवचन प्रत्यय)
- अर्थात चित्त के अनेक प्रकार।
अन्वय
- लोभसहगतचित्तानि = लोभेन सह गतानि चित्तानि
- अर्थात ऐसे चित्त जो लोभ (अतिशय तृष्णा या लालच) से जुड़े हुए हैं।
तात्त्विक अर्थ:
‘लोभसहगतचित्त’ वह चित्त होता है जो आसक्ति, तृष्णा, या लालच से प्रभावित होता है। यह चित्त अकुशल (अकुसल) होता है, क्योंकि यह लोभ (क्लेश) से उत्पन्न होता है और मोक्ष-मार्ग में बाधक होता है। अभिधम्म के अनुसार, लोभसहगतचित्त विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे—
- मिथ्या दृष्टि के साथ (दिट्ठिगतसंपयुत्तं)
- मिथ्या दृष्टि से रहित (दिट्ठिगतविप्पयुत्तं)
- संकल्पपूर्वक (ससङ्खारिकं)
- बिना संकल्प के (असङ्खारिकं)
संक्षिप्त सार
लोभसहगतचित्तानि = ऐसे चित्त जो लोभ (अतिशय तृष्णा, लालच) के साथ जुड़े होते हैं।
ये अकुशल चित्त होते हैं, जो मानसिक अशुद्धि और बंधन (संस्कार) को बढ़ाते हैं।
दोमनस्ससहगतं
- दोमनस्स + सहगतं
- दोमनस्स (Domanassa)
- दो (कष्ट, पीड़ा) + मनस्स (मन)
- अर्थात कष्टपूर्ण मानसिक अवस्था, दुख, चिंता, खिन्नता।
- बौद्ध दर्शन में यह मानसिक दुःख (मानसिक असंतोष) को दर्शाता है, जो द्वेष (द्वेष) और प्रतिघ (क्रोध) से जुड़ा होता है।
- सहगतं (Sahagataṁ)
- सह (साथ) + गत (गमनशील, संयुक्त)
- अर्थात जो किसी चीज़ के साथ संयुक्त हो या जिसमें सम्मिलित हो।
अन्वय
- दोमनस्ससहगतं = दोमनस्सेन सह गतं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो मानसिक दुःख (खिन्नता, उदासी, क्रोध) के साथ जुड़ा हो।
अर्थ
‘दोमनस्ससहगतं चित्त’ वह चित्त है जो दुख, खिन्नता, उदासी या मानसिक असंतोष के साथ उत्पन्न होता है। यह विशेष रूप से द्वेष (क्रोध) और प्रतिघ (विरोध) से संबंधित होता है। यह चित्त अकुशल (अकुसल) चित्त की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह मानसिक अशुद्धि और अशांति को बढ़ाता है। यह चित्त द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, जलन जैसी भावनाओं को जन्म देता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत रखता है।
संक्षिप्त सार
दोमनस्ससहगतं चित्त = ऐसा चित्त जो मानसिक दुख, खिन्नता या असंतोष से युक्त हो।
यह अकुशल चित्त होता है और द्वेष (क्रोध) से प्रभावित रहता है।
पटिघसम्पयुत्तं
पटिघ + सम्पयुत्तं
- पटिघ (Paṭigha)
- पटि (विपरीत, विरोध) + घ (√घट्) (टकराना, संघर्ष करना)
- अर्थात टकराव, विरोध, आघात, द्वेष, क्रोध, प्रतिघात।
- बौद्ध अभिधम्म में यह विशेष रूप से क्रोध और द्वेष (द्वेष) की मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- सम्पयुत्तं (Sampayuttaṁ)
- सम् (साथ) + पयुत्त (जुड़ा हुआ, संयुक्त)
- अर्थात जिसका किसी अन्य चीज़ के साथ घनिष्ठ संबंध हो, जो उससे जुड़ा हो।
अन्वय और अर्थ:
- पटिघसम्पयुत्तं = पटिघेन सम्पयुत्तं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो प्रतिघ (क्रोध, द्वेष) के साथ जुड़ा हो।
अर्थ
‘पटिघसम्पयुत्तं चित्त’ वह चित्त होता है जो क्रोध, विरोध, द्वेष, या मानसिक आघात से प्रभावित होता है। यह अकुशल (अकुसल) चित्त की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह मानसिक अशांति, संघर्ष और बंधन को बढ़ाता है। यह चित्त द्वेष (क्रोध) से उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति अशांत, क्रोधी, और हिंसक मानसिकता वाला बन जाता है। यह दोमनस्स (मानसिक दुःख) के साथ संबद्ध रहता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत और पीड़ित होता है।
संक्षिप्त सार
पटिघसम्पयुत्तं चित्त = ऐसा चित्त जो द्वेष, क्रोध और मानसिक आघात से युक्त हो।
यह अकुशल चित्त होता है और मानसिक अशांति एवं संघर्ष को जन्म देता है।
विचिकिच्छासम्पयुत्तमेकं
- विचिकिच्छा + सम्पयुत्तं + एकं
- विचिकिच्छा (Vicikicchā)
अभिधम्म दर्शन में ‘विचिकिच्छा’ अविद्या (अज्ञान) के कारण उत्पन्न संशयात्मक मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति धर्म (धम्म), बुद्ध, संघ, मार्ग आदि पर शंका करता है।
- सम्पयुत्तं (Sampayuttaṁ)
- सम् (साथ) + पयुत्त (संयुक्त, संबद्ध)
- अर्थात जो किसी अन्य चीज़ के साथ गहराई से जुड़ा हुआ हो।
- एकं (Ekaṁ)
- एक (एक मात्र, एक विशिष्ट)
- यहाँ यह एक प्रकार के चित्त को दर्शाता है।
अन्वय
- विचिकिच्छासम्पयुत्तमेकं = विचिकिच्छाय सम्पयुत्तं एकं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो विचिकिच्छा (संदेह, शंका) के साथ जुड़ा हुआ है और जो एक प्रकार का है।
अर्थ
‘विचिकिच्छासम्पयुत्तं चित्त’ वह चित्त होता है जो अज्ञानजनित संदेह, शंका, और असमंजस से प्रभावित होता है। यह अकुशल (अकुसल) चित्त की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह व्यक्ति को भ्रमित और अनिर्णायक बना देता है। इस चित्त में व्यक्ति को धम्म (धर्म), बुद्ध, संघ, निर्वाण, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग आदि पर संशय होता है। यह चित्त अज्ञान (अविद्या) का परिणाम होता है और मोहमूल चित्त (अज्ञानमूल चित्त) के अंतर्गत आता है।
संक्षिप्त सार
विचिकिच्छासम्पयुत्तमेकं चित्त = ऐसा चित्त जो संदेह, संशय और अज्ञान से प्रभावित हो।
यह अकुशल चित्त होता है और व्यक्ति को भ्रम, अनिर्णय एवं आध्यात्मिक प्रगति से दूर करता है।
उद्धच्चसम्पयुत्तमेकं
- उद्धच्च + सम्पयुत्तं + एकं
- उद्धच्च (Uddhacca)
- उद् (ऊपर, उच्च) + च्च (चंचलता, चपलता)
- अर्थात मन की अस्थिरता, चंचलता, व्याकुलता।
- अभिधम्म दर्शन में ‘उद्धच्च’ का अर्थ मन की अशांत और चंचल स्थिति से है, जिसमें मन इधर-उधर भटकता रहता है और एकाग्र नहीं हो पाता।
- यह मोहमूल (अज्ञानजन्य) चित्त का एक लक्षण है।
- सम्पयुत्तं (Sampayuttaṁ)
- सम् (साथ) + पयुत्त (संयुक्त, संबद्ध)
- अर्थात जो किसी अन्य चीज़ के साथ गहराई से जुड़ा हुआ हो।
- एकं (Ekaṁ)
- एक (एक मात्र, एक विशिष्ट)
- यहाँ यह एक प्रकार के चित्त को दर्शाता है।
अन्वय
- उद्धच्चसम्पयुत्तमेकं = उद्धच्चेन सम्पयुत्तं एकं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो उद्धच्च (मानसिक चंचलता, व्याकुलता) के साथ जुड़ा हुआ है और जो एक प्रकार का है।
अर्थ
‘उद्धच्चसम्पयुत्तं चित्त’ वह चित्त होता है जो मानसिक चंचलता, व्याकुलता, और ध्यान-अयोग्यता से प्रभावित होता है। यह अकुशल (अकुसल) चित्त की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह व्यक्ति को ध्यान, मनन, और एकाग्रता से दूर करता है। यह मोहमूल (अज्ञानमूल) चित्त के अंतर्गत आता है और अविपश्यना (सही दृष्टिकोण की कमी) का लक्षण है। इस चित्त में व्यक्ति एकाग्र नहीं रह पाता, उसका मन इधर-उधर भटकता रहता है, और वह किसी भी चीज़ पर ठहरकर विचार नहीं कर पाता। यह विशेष रूप से विपश्यना (सतत अवलोकन) और समाधि (एकाग्रता) की साधना में बाधा डालता है।
संक्षिप्त सार
उद्धच्चसम्पयुत्तमेकं चित्त = ऐसा चित्त जो मानसिक चंचलता और व्याकुलता से प्रभावित हो।
यह अकुशल चित्त होता है और व्यक्ति को एकाग्रता एवं आध्यात्मिक प्रगति से दूर करता है।
अहेतुकचित्तं
- अहेतुक + चित्तं
- अहेतुक (Ahetuka)
- अ (नकारात्मक उपसर्ग, ‘नहीं’) + हेतुक (हेतु सहित, कारण सहित)
- अर्थात जिसका कोई कारण (हेतु) नहीं हो।
- अभिधम्म दर्शन में “हेतु” से तात्पर्य “जड़ (root cause) या मूल कारक से है, जो किसी विशेष चित्त (मानसिक अवस्था) को उत्पन्न करता है।
- “अहेतुक” का अर्थ “बिना मूल कारण या जड़ कारक के उत्पन्न हुआ चित्त” है।
- चित्तं (Cittaṁ)
- चित् (सोचना, जानना, अनुभव करना) + त (भाववाचक प्रत्यय)
- अर्थात मनोवृत्ति, चित्त, मानसिक अवस्था।
अन्वय
- अहेतुकचित्तं = अहेतुकं चित्तं
- अर्थात ऐसा चित्त जो किसी मूल कारण (हेतु) से उत्पन्न नहीं हुआ हो।
अर्थ
‘अहेतुकचित्तं’ वह चित्त होता है जो किसी मूल कारण (हेतु) से उत्पन्न नहीं होता।
अभिधम्म में चित्त तीन प्रमुख श्रेणियों में बंटा होता है—
- सहेतुकचित्तं (जिसमें मूल कारण होते हैं)
- अहेतुकचित्तं (जिसमें कोई मूल कारण नहीं होते)
- लोभ, द्वेष और मोह के साथ जुड़े चित्त
अहेतुकचित्त मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं:
- अकुसलविपाकचित्त (अशुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न चित्त)
- कुसलविपाकचित्त (शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न चित्त)
- अहेतुककिरियाचित्त (ऐसा चित्त जो निष्क्रिय है, जैसे अरहंतों का हसितुप्पादचित्त)
विशेषताएँ:
- यह चित्त लोभ (राग), द्वेष (द्वेष) और मोह (अज्ञान) जैसे मूल कारकों से उत्पन्न नहीं होता।
- यह अधिकतर सेंसरी परसेप्शन (संवेदी अनुभूति) और अन्य प्रतिक्रियात्मक चित्तों से संबंधित होता है।
- पंचविज्ञान (चक्षु, स्रोत, घ्राण, जिह्वा, कायविज्ञान) अहेतुकचित्त के अंतर्गत आता है।
संक्षिप्त सार
अहेतुकचित्तं = वह चित्त जो बिना किसी मूल कारण (हेतु) के उत्पन्न हो।
यह सहेतुकचित्त से भिन्न है, क्योंकि इसमें लोभ, द्वेष, और मोह जैसे कारण मौजूद नहीं होते।
यह मुख्य रूप से संवेदी अनुभूतियों और निष्क्रिय प्रतिक्रियाओं से संबंधित होता है।
चक्खुविञ्ञाणं
- चक्खु + विञ्ञाणं
- चक्खु (Cakkhu)
- संस्कृत: चक्षु
- अर्थ: नेत्र, दृष्टि, आँख।
- अभिधम्म में ‘चक्खु’ का प्रयोग विशेष रूप से भौतिक नेत्र (Physical eye) और दृष्टि-संबंधी संज्ञान (Visual perception) के लिए किया जाता है।
- विञ्ञाणं (Viññāṇaṁ)
- वि + ज्ञा + ण (विशेष रूप से जानना)
- अर्थ: संज्ञान, चेतना, ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया।
- अभिधम्म में “विञ्ञाणं” का तात्पर्य चेतना (Consciousness) या संज्ञान (Cognition) से होता है।
अन्वय
- चक्खुविञ्ञाणं = चक्खुं निस्साय उत्पन्नं विञ्ञाणं
- अर्थात ऐसा संज्ञान (ज्ञान) जो चक्षु (आँख) के आधार पर उत्पन्न होता है।
अर्थ
‘चक्खुविञ्ञाणं’ वह चित्त होता है जो आँख के माध्यम से उत्पन्न होने वाले दृश्य बोध (Visual Consciousness) से संबंधित है। यह पंचविज्ञान (पाँच संवेदी चेतनाओं) में से एक है। जब कोई वस्तु आँखों के सामने आती है, तब चक्षु और रूप के संयोग से यह नेत्र-विज्ञान (Eye Consciousness) उत्पन्न होता है। यह सिर्फ देखने तक सीमित होता है, इसका अर्थ-बोध या मूल्यांकन मनोद्वारविज्ञान (Mānadvāra Viññāṇa) द्वारा किया जाता है। यह अहेतुकचित्तं (बिना मूल कारण के उत्पन्न होने वाला चित्त) की श्रेणी में आता है।
संक्षिप्त सार
चक्खुविञ्ञाणं = आँखों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली चेतना या संज्ञान।
यह पाँच संवेदी विज्ञानों में से एक है, जो देखने (दृश्य अनुभूति) से संबंधित है।
इसमें केवल “देखना” शामिल होता है, न कि वस्तु का मूल्यांकन या विश्लेषण।
चित्त
चित्त का अभिप्राय मन, चेतना या विज्ञान है। वह तत्व जो अनुभाव करता है उसे चित्त कहते है। यह स्थायी नहीं होता, बल्कि यह हर क्षण उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। चित्त वह है जो विषय को ग्रहण करता है। यह अपने विषय को ग्रहण करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। चित्त अकेला नहीं होता, बल्कि इसके साथ मानसिक कारक जुड़े होते है। परमत्थदीपनी में का गया है कि ‘चिन्तेतीति चित्तं’ अर्थात् जो विचार करता है, वह चित्त है।
कामावचर
कामावचर चित्त वे चित्त हैं जो कामधातु में कार्य करते हैं। यहां कामधातु का अभिप्राय उस अवस्था है जहाँ इंद्रियां रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श से के प्रभाव में रहती हैं।
रूपावचर
रूपावचर चित्त वे चित्त होते हैं, जो रूपध्यान के पाँच स्तरों में काम करते हैं। ये कामधातु से ऊपर और अरूपधातु से नीचे होते हैं।
अरूपावचर
निब्बानं— ‘वानतो निक्खन्तं ति निब्बानं’ अर्थात् वान नामक तृष्णा से रहित होने के कारण निर्वाण कहा जाता है। अत: जो तृष्णा का आलम्बन नहीं बनता है उसे निर्वाण कहते है।
चतुधा देसना (चार वर्गीकरण में धम्म देशना)
भगवान बुद्ध ने धम्म को इन चार वर्गों में विभाजित करके समझाया, जो कि अभिधम्म का आधार हैं। इसके साथ ही, बुद्ध ने चार आर्यसत्यों को भी इसी के माध्यम से प्रकट किया—
1. दुक्ख सच्च (दुःख सत्य) → रूप एवं चित्त का समावेश।
2. दुक्खसमुदय सच्च (दुःख उत्पत्ति का सत्य) → चेतसिकों में तृष्णा (तण्हा) का समावेश।
3. दुक्खनिरोध सच्च (दुःख निरोध का सत्य) → निब्बान का समावेश।
4.दुक्खनिरोधगामिनी प्रतिपदा सच्च (दुःख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग) → चित्त, चेतसिक, और अन्य कारक सम्मिलित।
चित्त को वर्गीकृत करने के लिए वेदना एक मुख्य कारक होती है—
इसमें वेदना को पाँच प्रकारों में विभाजित किया गया है—
1. सुख वेदना → शारीरिक सुख, जैसे आरामदायक जल में स्नान।
2. दुक्ख वेदना → शारीरिक पीड़ा, जैसे जलना, चोट लगना।
3.सोमनस्स वेदना → मानसिक आनंद, जैसे किसी प्रियजन से मिलना।
4. दोमनस्स वेदना → मानसिक दुःख, जैसे अपमानित होना।
5. उपेक्खा वेदना → न सुख, न दुःख, चित्त का अभिप्राय मन, चेतना या विज्ञान है।
आठ प्रकार के लोभ-सहगत चित्त:
| क्रम | चित्त का प्रकार | संवेदना (वेदना) | दृष्टि (दिट्ठि) | संकल्प (सङ्खार) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमनस्स-सहगत, दिट्ठि-संपयुत्त, असङ्खारिक | आनंद | मिथ्या दृष्टि | सहज |
| 2 | सोमनस्स-सहगत, दिट्ठि-संपयुत्त, ससङ्खारिक | आनंद | मिथ्या दृष्टि | संकल्प सहित |
| 3 | सोमनस्स-सहगत, दिट्ठि-विप्पयुत्त, असङ्खारिक | आनंद | मिथ्या दृष्टि रहित | सहज |
| 4 | सोमनस्स-सहगत, दिट्ठि-विप्पयुत्त, ससङ्खारिक | आनंद | मिथ्या दृष्टि रहित | संकल्प सहित |
| 5 | उपेक्षा-सहगत, दिट्ठि-संपयुत्त, असङ्खारिक | उपेक्षा | मिथ्या दृष्टि | सहज |
| 6 | उपेक्षा-सहगत, दिट्ठि-संपयुत्त, ससङ्खारिक | उपेक्षा | मिथ्या दृष्टि | संकल्प सहित |
| 7 | उपेक्षा-सहगत, दिट्ठि-विप्पयुत्त, असङ्खारिक | उपेक्षा | मिथ्या दृष्टि रहित | सहज |
| 8 | उपेक्षा-सहगत, दिट्ठि-विप्पयुत्त, ससङ्खारिक | उपेक्षा | मिथ्या दृष्टि रहित | संकल्प सहित |